श्री गणेशाय नमः
श्री श्याम देवाय नमः
आध्यात्मिक पेंशन से अभिप्राय है— आत्मिक शांति या आध्यात्मिक शांति।
यह सिर्फ प्रभु भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। परंतु हमारे समाज में मनुष्य की यह विडंबना ही है कि वह अध्यात्मिक पेंशन को जानता ही नहीं।
वह सिर्फ मौद्रिक पेंशन को ही जानता है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव पर अशांत एवं असंतुष्ट दिखाई देता है। वह अपने जीवन का अधिकांश समय मौद्रिक पेंशन को कमाने में गंवा देता है परंतु वह अपने आंतरिक संसार में बैठे दुश्मनों जैसे— दुराग्रह, अहंकार, मोह, माया इत्यादी के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं लड़ता। इसलिए उसे दोहरी पेंशन के रूप में आध्यात्मिक पेंशन नहीं मिल पाती।
यह पेंशन जीवन में मनुष्य को सम अवस्था के रुप में प्राप्त होती है। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। जन्म- जन्मांतर से जमा हो रहे कर्मफल के कीचड़ में सना मानवीय मन सांसारिक माया के वशीभूत होकर असहज जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होता है। वह अज्ञानी, मानव रुपी चोला धारण करने के बाद उस निरंकारी ब्रह्म का स्मरण करना भूल जाता है।
किसी भी प्रकार का कर्म, शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है। इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहें। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है, वह जीवित रहते हुए भी अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभाशुभ कर्म और शरीर बार-बार नहीं प्राप्त होता।
विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठादि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए, ज्ञान की रक्षा ध्यान-योग के लिए तथा ध्यान-योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकती तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा।
यदि यहां इसी लोक में नर्करूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई तो औषधिविहीन देश (परलोक) में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा? बुढ़ापा तो बाघिन के समान है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे-धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान कष्ट शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं। इसलिए इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत्प्रयास किया जाए।
जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, विपत्तियां सामने नहीं आती और शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती, तब तक ही आत्मकल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक ही तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक् प्रयत्न किया जा सकता है। कोषागार में आग लग जाने पर मूर्ख ही कुआं खोदता है अर्थात् मानव अपने अंतिम समय में ही आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ऐसे पर्यत्न का क्या लाभ?
गरुड़ पुराण के अनुसार— मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से, समय को नहीं जान पाता। वह दुख-सुख तथा आत्महित को भी नहीं जानता। पैदा होने वालों को, रोगियों को, मरने वालों को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर (मनुष्य मोहरुपी मदिरा को पीकर जन्म- मरणादि दुख से युक्त संसार से) भी नहीं डरता।
सम्पदाएं स्वप्न के समान हैं, यौवन पुष्प के सदृश है, आयु चंचल बिजली के तुल्य नष्टप्राय: है। ऐसा जानकर भी किसको धैर्य हो सकता है। सौ वर्ष का जीवन भी बहुत कम है क्योंकि परिमित आयु का आधा भाग रात्रियों में ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्धावस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आयु सौ वर्ष मानी गई है। आयु का आधा भाग रात्रियों में ही समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीत जाता है, कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायी मृत्यु से प्राप्त कष्ट तथा राजसेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता भी है, वह जलतरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है।
मृत्यु दिन- रात वृद्धावस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वह प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है, जैसे सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति सभी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता, तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत् ही है। कदाचित् वायु को बांधकर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सूत्रादि में पिरोया जा सकता है किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसके प्रभाव से पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है, फिर इस शरीर के संबंध में तो बात ही क्या? पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु- बांधव मेरे हैं। इस प्रकार मैं-मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति कालरूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है।
यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, मैंने अच्छा किया है— इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। इसलिए कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करना है, उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती।
वृद्धावस्था पथ- प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक हैं, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक “भगवान” का स्मरण क्यों नहीं करता? वह क्यों नहीं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है? तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित, विषयरूपी घृत में डूबे, राग- द्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाये गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह संसार। इतना होने के बावजूद भी मनुष्य इस सांसारिक मोह- माया का परित्याग नहीं कर पाते और दुख के भागी बन कर आध्यात्मिक पेंशन को प्राप्त नहीं कर पाते।
मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है, उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती हैं। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली, बंसी के कांटे को नहीं देखती, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ मानव शरीर, यम की बाधा को नहीं देखता है। इसलिए मनुष्य को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए।
यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो प्रभु- भक्ति के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि आसक्ति रुपी व्याधि की औषधि प्रभु- भक्ति है। युवा तथा प्रौढ़ावस्था में मनुष्य भौतिक व्यसनों और सुख- सुविधाओं से मानसिक अशांति को कुछ समय के लिए शांत कर लेता है, परंतु वृद्धावस्था में जब शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है, तब वह उनसे शांति नहीं पाता। तब उसे अध्यात्मिक पेंशन की आवश्यकता होती है।
यह आध्यात्मिक पेंशन भी मनुष्य को अपने आंतरिक संसार के दुश्मनों से लड़ कर कमानी पड़ती है। परंतु जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए था, उसके संदर्भ में तो वह उद्योगहीन होकर बैठा रहा। जहां जागते रहना चाहिए था, वहां सोता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि- जो मनुष्य अहित में हित, अनिश्चित में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह मनुष्य अपने मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता अर्थात् वह जानता तो है लेकिन माया रूपी अंधकार ने उसे घेर रखा है। इसलिए वह देखते हुए भी गिर जाता है, सुनते हुए भी सद्-ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता, सद्ग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता क्योंकि वह प्रभु-भक्ति से विमुख है।
प्रत्येक धर्म में इसकी प्राप्ति के नियम लगभग एक समान ही होते हैं। जैसे— सच्चे मूल्यों से अर्जित जीवन यापन, दया एवं करुणा, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, अहिंसा, सत्य और सही दृष्टिकोण इत्यादि। पतंजलि ने इन्हें अष्टांग योग के रूप में परिभाषित किया है। इन जीवन मूल्यों को अपनाने से मनुष्य धीरे-धीरे कर्म फलों से मुक्ति पाकर सम स्थिति में पहुंचकर आध्यात्मिक पेंशन के रूप में शांति का अनुभव करने लगता है और इस प्रकार इस पेंशन द्वारा मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।
लेकिन इस धरा पर मनुष्य को हजारों चिंताओं ने अपना ग्रास बना रखा है, जिसके कारण वह अध्यात्म रूपी नौकरी कर ही नहीं पाता। मनुष्य को इस सार्वभौमिक सत्य को समझना होगा कि अगर उसने मौद्रिक पेंशन के साथ- साथ आध्यात्मिक पेंशन का सुख भी प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रभु-भक्ति करनी ही पड़ेगी। वरना वह जन्म- जन्मांतर के चक्रों से छुटकारा नहीं पा सकता।
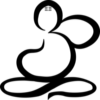
Jai Shree Radhe Radhe Shyam 🔥🔥🔥👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋Manjit Kumar Rohilla