श्री गणेशाय नमः
श्री श्याम देवाय नमः
मनुष्य अपने जीवन में अनेक चरित्र एक साथ निभाता हुआ अपने पथ पर अग्रसर होता है। घर में वह पारिवारिक संबंधों से जुड़ा होता है। घर के बाहर सामाजिक संबंध उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इन संबंधों से जन्म लेती इच्छाएं उसकी मानसिक शांति को छिन्न -भिन्न करने का कार्य करती हैं, क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। यह चंचल मन ही अशांति का मूल कारण है।
मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाएं इस चंचल मन की ही देन हैं, जो उसे दिन-रात व्यस्त रखती हैं। कभी शांत नहीं होने वाली इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे हम अंधे होकर भागते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का एक बड़ा भाग इनकी पूर्ति में ही व्यय हो जाता है। एक इच्छा पूरी होते ही हम दूसरी इच्छा अपने मन में पाल लेते हैं। हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है।
सम्बन्धों का मोह मनुष्य को भ्रम के संसार में ले जाता है। वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते-करते पाप का भागी भी बन जाता है, क्योंकि मनुष्य की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छाएं बलवती होती जा रही हैं। इसलिए उसके जीवन में मोह माया की तृष्णा निरंतर बढ़ रही है। जल्दी पाने की अधीरता शांति के मार्ग में बाधक बन रही है और व्यग्रता मनुष्य को तनावशील बना रही है।
मोह-माया जीवन के क्षणिक आनंद हैं। ये सब कुछ जानते- समझते हुए भी वह अपने सम्बन्धों के पोषण के लिए गलत कार्य करते हुए भी नहीं हिचकता। मोह और माया से ग्रस्त मानव का पागलपन दूसरों के लिए सदैव कष्टकारी साबित होता है, किंतु समाज में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मनुष्य की इस प्रवृत्ति को गृहस्थ, सामाजिक और जिम्मेदारी जैसे भारी शब्दों से महिमामंडित तो कर दिया, परंतु उसके स्व तत्व की उपेक्षा की कभी चिंता नहीं की।
इच्छा पूर्ति के लिए मोह- माया में फंसे हुए मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है। उन भौतिक वस्तुओं का सुख तो अन्य लोग भोगते हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जो अनजाने में पाप कर बैठा, उनका दंड उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। संसाधनों की बढ़ोतरी जीवन में सुख का क्षणिक आनंद दे सकती हैं, लेकिन इनसे चिरस्थायी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इच्छाओं की प्रकृति यदि बुरी हो तो वह हमें पाप की राह पर धकेल देती है। बुरी इच्छाओं का वेग मानवीय गुणों को नष्ट कर देता है, जिससे मानव अपने सद्गुणों को भूलकर दुर्गुणों यथा दंभ और मद्यपान का शिकार हो जाता है। मोह- माया में केवल हासिल करने की ललक रहती है। स्वयं के स्वार्थ के आगे सब कुछ गौण होने लगता है, जिससे वह कर्तव्य पथ से भटक जाता है। वह इच्छाओं की पूर्ति में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने तन के भीतर का स्व: दिखाई ही नहीं देता।
इच्छाओं के स्वच्छंद आकाश का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं ही तृष्णा बढ़ाती हैं। तृष्णाओं के कारण ही मनुष्य स्वार्थ की संकीर्णता से ग्रस्त हो जाता है।
मानव के लिए चंचल मन में उठ रहे इच्छाओं के वेग को रोकना कठिन है, लेकिन अपने मन को एकाग्र करके उन्हें सीमित तो किया जा सकता है। इच्छाएं यदि नेक हों, समाज व राष्ट्र हित में हो तो वे एक अद्भुत शक्ति का कार्य करती हैं और यदि वे ईर्ष्या, बुराई एवम् घृणा जैसे कलुषित भावों में पली-बढ़ी हों, तो समाज, राष्ट्र के साथ ही स्व विनाशकारी साबित होती हैं।
इच्छाओं को सीमित करने में ही जीवन का सुख छुपा है। जब हमें भौतिक वस्तुओं से लगाव नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में उनको पाने की लालसा भी खत्म हो जाएगी, जिससे हमारे जीवन में तृप्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा, जो हमें चिरस्थाई शांति प्रदान करेगा। तृप्ति के कारण ही हम अपने चंचल मन को शांत करके अपनी उर्जा को सद्कर्मों में लगा सकते हैं।
आज के दौर में इच्छाएं इतनी बलवती हो गई है कि वे हिंसा और दुराचारों का मुख्य कारण बनती जा रही हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी बेलगाम होती इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। समस्या का समूल समाधान परमात्मा के ध्यान में ही निहित है। इससे मन विचलित नहीं होता। गलत विचारों, इच्छाओं को नष्ट कर मन में शुद्धता आती है, तो निश्चित ही मन की शांति के साथ-साथ मानसिक सुख की अनुभूति होती है।
मन में तभी शुद्धता आएगी जब हम अपने अंदर पनपती हुई इच्छाओं को नष्ट कर दें। शांति की स्थापना के लिए शून्यता का सिद्धांत जरूरी है, अर्थात् हमारा मन खाली होगा, तभी उसमें कुछ समा सकता है। हमें अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए चित्त में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा होता है, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप मन के प्रभाव से परे हो जाते हैं और स्वंय में चले जाते हैं। जिससे हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आने लगते हैं। प्रसन्नता से हमारी चेतना जाग्रत होती है।
जब मन सभी संस्कारों और अवधारणाओं से मुक्त होता है, तो आप इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब आपको ज्ञात होता है कि सब कुछ बदल रहा है— सभी संबंध, व्यक्ति, शरीर, भावनाएं, अचानक मन जो दुख से चिपका है, आपके पास वापिस आता है। जिससे आपके स्व का पता चलता है। आपके स्वयं से स्वयं तक की वापसी आपको दुख से मुक्ति देकर संतोष प्रदान करती है।
यह ठीक उसी प्रकार होता है कि— जब कमरा बहुत गर्म हो जाता है, तो आप शरीर को कुछ आराम देने के लिए वातानुकूल का प्रयोग करते हैं। मन के लिए ए. सी. ध्यान है। अपने मन को पूर्ण विश्राम देने के लिए जब आप ध्यान करते हैं, तो आप मन के प्रभाव से परे हो जाते हैं और स्वयं में चले जाते हैं। जब आप स्वंय में जाते हैं तो आपको स्व का बोध होता है। जिससे आपकी इच्छाओं पर लगाम लग जाती है।
ध्यान ही हमारे कष्टों को कम कर हमारे जीवन की राह को सुगम कर सकता है। अतः इच्छाओं रूपी व्यर्थ की भावनाओं के पीछे दौड़ने की बजाय हमारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। यह जगत् तो चार दिनों की चांदनी और भ्रम का मायाजाल है। जिसे एक न एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन ईश्वर अविनाशी, अजर और अमर है। उसका सान्निध्य ही अतृप्त इच्छाओं से पीड़ित मनुष्य को सही राह दिखा कर इस धरा पर उसके जीवन को सार्थक करता है।
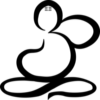
I loved you even more than you’ll say here. The picture is nice and your writing is stylish, but you read it quickly. I think you should give it another chance soon. I’ll likely do that again and again if you keep this walk safe.
helloI like your writing very so much proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this space to unravel my problem May be that is you Taking a look forward to see you
helloI really like your writing so a lot share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this house to unravel my problem May be that is you Taking a look ahead to see you