श्री गणेशाय नमः
श्री श्याम देवाय नमः
किसी के जीवन में कांटे बो कर हम खुशियों के फूलों की कल्पना नहीं कर सकते। खुशियों के फूल हमारे कर्मों की खाद- पानी से पल्लवित व पुष्पित हृदयरूपी क्यारी में ही खिल सकते हैं। मन की पवित्रता और सकारात्मक विचारों से बुरे से बुरे कार्य भी अच्छे में परिणत हो सकते हैं। मन की मलिनता दूसरों को क्षति पहुंचाने की बजाय अपने ही प्रारब्ध व भविष्य के पंख कुतरने को विवश करती है। हमारे विचारों और कर्मों के मंथन से ही खुशी या दुख की रचना होती है।
हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों से ही हमारे अगले जन्म में खुशियों के फूल खिलते हैं। वरना क्या कारण है कि एक ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति से, जल-वायु के सानिध्य से पोषित होकर कालांतर में उन बीजों में से एक विष बनता है व दूसरा अमृत। अर्थात् एक ही माता-पिता की संतान होने के बाद भी किसी की जीवन रूपी बगिया में खुशियों के फूल खिलते हैं और किसी को दुख और कठिनाइयों का सामना करते हुए नरकीय जीवन जीना पड़ता है।
यदि पालन पोषण से ही सारे संस्कार आते, तो उसी खाद अथवा मिट्टी- पानी का सेवन कर एक विष व दूसरा अमृत कैसे बन गया? ठीक उसी प्रकार जैसे—एक भरी- पूरी कक्षा में एक छात्र स्वर्ण पदक विजेता व दूसरा अनुत्तीर्ण कैसे हुआ? जबकि दोनों को शिक्षा देने वाले गुरुजन समान थे। दरअसल विगत का कर्म फल ही वर्तमान में प्रारब्ध का बीज बनकर विष- अमृत के रूप में परिभाषित होता है।
व्यर्थ नहीं होते कर्म— जैसे हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है। एक ऐसा सुंदर यंत्र जिसके साथ उसकी स्वामी आत्मा विलक्षण रीति से अभिन्न हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का यंत्र है। परमात्मा उसके अंदर निवास करता है, उसका उपयोग करता है। व्यक्ति को परमात्मा का जो उसके अंतस में निवास करता है, अच्छा और विश्वस्त यंत्र बनना चाहिए और प्रत्येक कर्म, विचार और वाणी उसको समर्पित करनी चाहिए।
कर्म, शरीर, वाणी और मन से किए जाते हैं। प्रत्येक कर्म का नियत परिणाम होता है। कारण, कार्य- विधान अपरिवर्तनीय हैं। कर्म के संबंध में गौतम बुद्ध के जीवन का एक वाक्य स्मरण हो आया।
गौतम बुद्ध एक आम के पेड़ के नीचे समाधि में बैठे हुए थे। आम तोड़ते समय एक बच्चे के हाथों से फेंका गया पत्थर गौतम बुद्ध के सिर पर जा लगा। सिर से खून निकलने लगा।
बुद्ध परेशान दिखने लगे और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। जब बच्चे ने देखा तो उसे लगा कि अब तो बुद्ध उसे डांट फटकार लगाएंगे। वह डरा- सहमा खड़ा था। उस बच्चे ने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा। बच्चा उनसे कुछ कहता, उसके पहले ही बुद्ध बोला— तुमने आम को पत्थर मारा तो आम ने तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन जब तुम्हारा पत्थर मेरे सिर पर लगा तो तुम भयभीत हो गए। क्योंकि मैंने तुम्हें भय दिया। लेकिन ये सच नहीं है— जिस प्रकार पेड़ का धर्म मीठे फल देना है, उसी प्रकार संन्यासी का धर्म क्षमा करना है। इसलिए तुम जाओ, हम तीनों ने अपने- अपने स्वभाव के अनुसार कर्म किया।
इसलिए हमें परिणाम की चिंता किए बगैर कर्म करते रहना चाहिए। परिणाम कारण में वैसे ही निहित रहता है, जैसे बीज में वृक्ष। पानी को सूर्य सुखा देता है, यह अन्यथा नहीं हो सकता। उष्णता और पानी के मिलने से परिणाम होगा ही। यही बात सब के साथ है। परिणाम कारण के गर्भ में रहता है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो संपूर्ण जगत अपने विविध अंगों में कर्म के अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार विकसित होता दिखलाई पड़ेगा।
वेदांत में कर्म के इसी सिद्धांत का निरूपण किया गया है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं हो सकता। कर्म करना और उसके परिणाम से बच जाना या किसी ऐसे परिणाम की आशा करना, जो किसी दूसरे कर्म से हो सकता है, संभव नहीं है। निश्चित कर्मों का उनके अनुरूप परिणाम होना अनिवार्य है। कर्म के विधान से सच्चा कर्म स्वातंत्र्य उत्पन्न होता है। कर्म की प्रकृति एवम् गुणधर्म के अनुसार ही जीव भावी जीवन जीने के लिए विवश होता है।
यदि अतीत के कर्मफल से वर्तमान का निर्माण संभव है तो वर्तमान के सदुपयोग से उसी अनुपात में भविष्य का सुखद निर्माण भी।
सदविचारों के समुचित दिशा में प्रसार से हर्ष का परिवेश बनता है, जबकि उन्हीं विचारों का अनुचित दिशा में नकारात्मक उपयोग खुशियों के महल को तहस-नहस कर सभी प्रकार के दुखों, क्लेशों व विपत्तियों का कारण भी बन सकता है। जानबूझकर जो षड्यंत्र अथवा कुचक्र किसी ओर के लिए रचे जाते हैं, वे परोक्षत: स्वंय को ही षड्यंत्रों के भवंर में डुबो देने का उपक्रम करते हैं। किसी का कुछ भी अनिष्ट सोचने से पहले स्वंय को उसके स्थान पर रखकर देखें। यह दुर्लभ शरीर बहुमूल्य है। इसलिए इस मन को इधर-उधर भटकाने की बजाय अपने कर्मों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, न कि रात- दिन कुचिंतन के मार्ग पर अग्रसर हो अनाप-शनाप लिख, बोलकर, कोर्ट- कचहरियों के चक्कर में फंसे दुर्लभ जीवन गवाने में लगाना चाहिए।
जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है, किंतु उसको नष्ट नहीं करता। जैसे दूध दुहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दुहता है। वैसे ही हमें सबके हित को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों को संचित करते रहना चाहिए। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी जो अच्छे कर्म के भागी नहीं बनते, वे इस संसार में शोक के पात्र हैं और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत् विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में खुशियों रूपी फूल कभी नहीं खिलते। ऐसे मनुष्य वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिरकाल में कोहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।
शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है, वह अपने कर्मों को संचित करता हुआ अपने आने वाले जीवन व जन्म में खुशियों रूपी बगिया की जमीन तैयार करता हुआ, बन्धु- बान्धवों, मित्रों का ख्याल रखता हुआ, परिवार का भरण- पोषण करता हुआ, धर्म में प्रवृत्त होता हुआ, दुर्जनों की संगति का परित्याग करता हुआ, साधुजनों की संगति करता हुआ और दिन-रात पुण्य कर्मों का संचय करता हुआ, अपनी मानवीय जीवन यात्रा में खुशियों के फूल संग्रहित करता हुआ, अपनी यात्रा पूर्ण करता है।
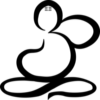
I have been diligently seeking information on this subject for quite some time, and yours is the most compelling piece I have come across thus far. Nevertheless, with that being stated, what is the final verdict? Are you certain regarding the supply?